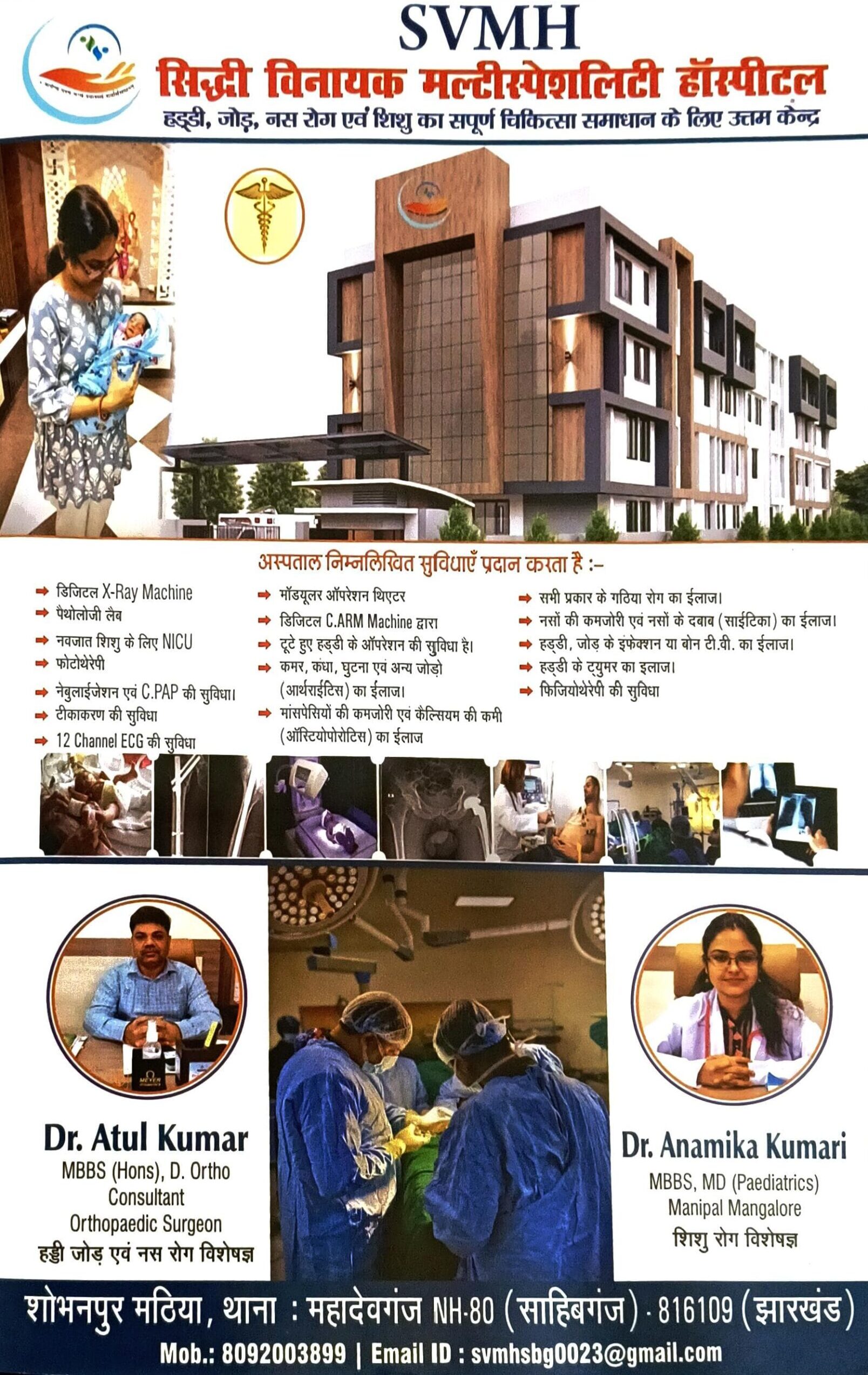-
परमाणु शक्ति की चमक के पीछे झारखंड के जादूगोड़ा का अंधेरा
Jaduguda (Jamshedpur): भारत आज दुनिया के उन गिने-चुने नौ देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इसे देश की रणनीतिक ताक़त और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस परमाणु ताक़त की बुनियाद पर खड़ा एक ऐसा गाँव भी है, जो खुद इसके दुष्परिणाम झेल रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम ज़िले में स्थित जादूगोड़ा, वह गाँव है जहाँ से देश को यूरेनियम मिलता है, लेकिन बदले में इस गाँव को मिली है बीमारियाँ, जन्मदोष, बाँझपन और एक अदृश्य, लेकिन जानलेवा रेडिएशन की मार।
झारखंड के जादूगोड़ा क्षेत्र की यूरेनियम खदानें
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम खान है, जिसकी खुदाई 1967 में शुरू हुई। इसके बाद 25 किलोमीटर के दायरे में भटिन, नारवा पहाड़, तुरमडीह, बांधुरंग, मोहुलडीह और बगजता जैसी कई और खदानें और प्रोसेसिंग संयंत्र विकसित हुए। इन खदानों और मिलों का संचालन सरकारी उपक्रम यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) द्वारा किया जाता है। UCIL का कहना है कि इसने खनन के लिए कुशल कार्यबल तैयार किया, लेकिन स्थानीय समुदायों का आरोप है कि उनकी ज़िंदगी और ज़मीन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई है। भारत सरकार की योजना के अनुसार 2031-32 तक घरेलू यूरेनियम उत्पादन लगभग दस गुना बढ़ाना है, लेकिन तब तक निर्यात से भरपाई के लिए उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के साथ अनुबंध हैं।
जादूगोड़ा की पहाड़ियों पर बने टेलिंग तालाबों (mining tailing ponds) से चारों ओर रेडियो एक्टिव धूल उड़ती रहती है, जिसे स्थानीय लोग स्वास्थ्य के लिए ख़तरा मानते हैं। टेलिंग तालाब वह जगह होती है जहाँ यूरेनियम अयस्क से येलोडकेक (पीला पदार्थ) निकालने के बाद बचा छर्रा और मिलावटी विलयन जमा किया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये असीमित मात्रा में दूषित तलछट बरसात में नदियों और भूजल में मिल जाते हैं, जिससे पानी और मिट्टी प्रदूषित हो रही है। कुल मिलाकर, इन खदानों से निकले जहरीले पदार्थों ने आसपास के पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

यूरेनियम का स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर
खनन प्रभावित इलाकों में रहने वाले आदिवासी ग्रामीणों ने हमेशा से ही अपनी पीड़ा बयान की है।
जादूगोड़ा निवासी 35 वर्षीय आगनु मुर्मू ने अल जज़ीरा से कहा, “उन्होंने मेरी जमीन ले ली और मुझे कैंसर दे दिया”।

52 वर्षीय राखी मुर्मू बताती हैं कि वह टेलिंग तालाब के पास अपने बच्चों को खेलने देती थीं और उसमें पकड़कर मछलियाँ पकड़ा करती थीं, अब पता चला कि वे नदियाँ रेडियोधर्मी हो गई हैं।
इसी गाँव की 42 वर्षीय जिंगी बिरुले को जन्म से दोनों हाथों में मध्यमा और अनामिका उंगलियाँ जुड़ी हुई पैदा हुईं; उनकी असामान्य अवस्था के चलते उन्हें सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा।

दुंगड़िह ग्राम की नमिता सोरेन ने साफ कहा कि यह “रेडियो एक्टिव तत्व हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है” और अब “बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं या लोग कैंसर से पीड़ित”।

इन गांवों के बच्चे और युवा भी पीड़ित हैं। बांगो गांव में 18 वर्षीय राकेश गंभीर शारीरिक विकलांगता के कारण व्हीलचेयर में है।

तेज़गति से फैलती रेड़िएशन से प्रभावित होने पर गाँव की कई लड़कियाँ बाँझ हो रही हैं, उनके गर्भपात आम हो गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी तथा स्वतंत्र अध्येताओं की रिपोर्ट बताती है कि आसपास की महिलाओं में 1998-2003 के बीच 18% से ज़्यादा बार गर्भपात हुए और करीब 30% महिलाओं को गर्भधारण में कठिनाई हुई।
नरवा पहाड़ यूरेनियम खदान से लगभग एक किलोमीटर दूर डुंगरीडीह गाँव में अनामिका ओराओम अपनी माँ नागी ओराओम के साथ। अनामिका के चेहरे पर एक घातक ट्यूमर है, लेकिन परिवार सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकता। उसकी माँ भी कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं।

खनन में लगे स्थानीय मजदूरों की भी हालत दयनीय है। तुरमडीह की एक यूरेनियम खान में काम करने वाला मजदूर अपने विकृत पैरों के कारण मुश्किल से चल पा रहा है।

ग्रामीण लगातार स्वास्थ्य-जांच और क्षतिपूर्ति की माँग कर रहे हैं, लेकिन UCIL का कहना है कि खनन और रेडिएशन नियंत्रण में हैं और स्वास्थ्य पर इसका असर नहीं हुआ”। इन्हीं विरोध-प्रदर्शनों के बीच यूसीआईएल ने अपने बयान में इसे आधारहीन आरोप करार दिया है।
वैज्ञानिक रिपोर्ट्स करते हैं सरकारी दावों को ख़ारिज
सरकारी अधिकारी और UCIL लगातार इन आरोपों का खंडन करते रहे हैं। टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार यूसीआईएल और परमाणु ऊर्जा आयोग बार-बार कहते रहे हैं कि जादूगोड़ा की खानें सुरक्षित रूप से संचालित हो रही हैं। हालाँकि 2014 में झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश भी दिया था। वहीं, स्वतंत्र शोध बताते हैं कि प्रदूषण की आशंकाएँ वास्तविक हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रो. दिपक घोष के 2009 के अध्ययन ने पाया कि जादूगोड़ा के पास बहने वाली सबर्नरेखा नदी और आसपास के कुओं में अल्फा-कणों का उत्सर्जन विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 192% अधिक था। जापानी वैज्ञानिक हिरोआकी कोइदे ने भी परीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि खदानों के नज़दीकी गांवों में रेडिएशन स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों से लगभग दस गुना अधिक है। परमाणु भौतिकीविद् सुरेंद्र गडेकर ने 2001 में 9,000 ग्रामीणों का सर्वे किया और पाया कि खदान क्षेत्र में रेडिएशन सामान्य से 5-6 गुना ज़्यादा था, साथ ही दूरदर्शिता रोग, कैंसर और जन्मदोष के मामले विश्लेषित किए गए।
ये अध्ययन उच्च रेटगाथाओं की पुष्टि करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में उल्लेख है कि आसपास की महिलाएं बाँझपन, जन्मदोष और अन्य गंभीर बीमारियों से लगातार पीड़ित हो रही हैं; कुछ जगह रेडिएशन स्तर सुरक्षित सीमा से 60 गुना तक ऊँचा पाया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य समस्याओं को गरीबी या स्वच्छता की कमी का परिणाम बताया है, लेकिन प्रभावित समुदाय इस पर विश्वास नहीं करता। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कई चेतावनियाँ दबाई गईं या खारिज की गईं।
इन तथ्यों से यह प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रीय परमाणु नीति के लिए यह दाम बहुत अधिक नहीं है? नीति-निर्माताओं पर जनता का दबाव बढ़ाने और समस्याओं की जड़ तक पहुँचने के लिए विशेषज्ञ कई सिफारिशें दे रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक मेडिकल और रेडिएशन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। प्रभावित महिलाओं के लिए मुफ्त बांझपन जांच और परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। खनन इलाकों में रेडिएशन की निरंतर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। सरकार को इसे केवल तकनीकी या आर्थिक मुद्दा न मानकर पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और मानवाधिकार के संदर्भ में देखना चाहिए।
स्वास्थ्य सर्वेक्षण और रेडिएशन परीक्षण: प्रभावित आबादी की नियमित जाँच हो। मुफ़्त बांझपन जांच: प्रभावित महिलाओं को निशुल्क बांझपन जांच और परामर्श उपलब्ध कराया जाए। सख्त मॉनिटरिंग: खदानों और आसपास की हवा-पानी में रेडिएशन का कड़ाई से परीक्षण एवं नियंत्रण हो। समग्र नीति: इस समस्या को सिर्फ तकनीकी मुद्दा न मानकर बड़े सामाजिक-पर्यावरणीय सवाल की तरह हल किया जाए।
बात सिर्फ एक गांव या क्षेत्र की नहीं है; यह राष्ट्रीय परमाणु नीति के मानव और पर्यावरणीय प्रभावों पर बहस है। एक स्थानीय एक्टिविस्ट ने सवाल उठाया है कि “झारखंड ने देश को यूरेनियम दिया, देश ने हमें क्या दिया”, इस संतुलन को देखना जरूरी है। वैज्ञानिक रिपोर्ट और स्थानीय गवाहियों के मद्देनज़र नीति-निर्माताओं को पूर्ण समीक्षा कर उचित पारदर्शी कदम उठाने पर मजबूर किया जाना चाहिए ताकि जादूगोड़ा और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीणों का भविष्य सुरक्षित रहे।
ये भी पढ़ें: Dhanbad में अवैध खनन के दौरान धंसी चाल, 10 से अधिक मजदूरों के फंसे होने की आशंका